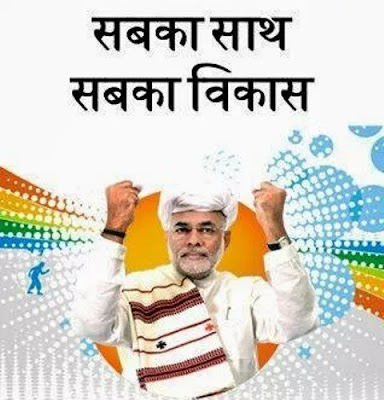ये हर बात पर जंग क्यों छिड़ी है?
शायर वसीम बरेलवी ने एक शेर में पते की बात कह दी है।
“अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उस को छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा।“
क्विंट की पत्रकार स्तुति मिश्रा ने ट्वीटर पर छह छोटे शब्द लिखने से पहले वसीम बरेलवी के इस शेर को सुना होता, तो शायद वो कभी न लिखतीं।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार रात खुद को स्वाइन फ्लू होने की बात ट्वीटर पर बताई। इसके रिएक्शन में पत्रकार स्तुति मिश्रा ने जो लिखा, वो बेशक गलत है। स्तुति मिश्रा ने लिखा – “People die of swine flu, right?”
पत्रकार ने इन शब्दों को लिखते वक्त क्या सोचा होगा; ये तो वही जानें। पर इन शब्दों का इशारा भद्दा है। इन शब्दों से निकले अर्थ पत्रकार को असंवेदनशील इंसान साबित कर रहे हैं।
इन छह शब्दों ने एक पत्रकार के हजारों अच्छे शब्दों का काम तमाम कर दिया।
क्विंट ने स्तुति मिश्रा की असंवेदनशील और अपरिपक्व टिप्पणी के लिए माफी मांगी और अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
पर इससे काम तो बनता नहीं है। जो तीर स्तुति मिश्रा के कमान से निकला है, वो लौटने वाला तो नहीं।
स्तुति मिश्रा के असंवेदनशील कमेंट ने एनडीटीवी की सीनियर पत्रकार सुनेत्रा चौधरी की एक पुरानी गलती को भी उभार दिया है। करीब दस साल पहले 2009 के अक्टूबर महीने में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वाइन फ्लू हुआ था।
अखबारों में ये खबर छपी, तब सुनेत्रा चौधरी खबर सुनकर काफी एक्साइटेड फील करने लगीं। उन्होंने अपनी ये खुशी ट्वीटर पर तुरंत जाहिर भी की।
अब जबकि स्तुति मिश्रा ने अमित शाह की बीमारी को लेकर भद्दा कमेंट किया, तो लोगों ने सुनेत्रा चौधरी के उस पुराने कमेंट को कब्र से निकालकर जिंदा कर दिया।
स्तुति मिश्रा के छह शब्दों के बहाने मीडिया के दो संस्थान निशाने पर आ गए हैं।
एक झटके में क्विंट और एनडीटीवी की “अच्छी-बुरी” पत्रकारिता को “सिर्फ बुरी” पत्रकारिता के खांचे में भरने की मुहिम चालू है।
शब्दों के खिलाड़ियों को संवेदनशील होना ही चाहिए। क्रिकेट की शब्दावली में कहें, तो ये उसी तरह है। जैसे किसी टीम का बॉलर आखिरी ओवर की आखिरी बॉल फेंक रहा हो। और उसने तब नो बॉल फेंकी, जब विरोधी टीम को मैच जीतने के लिए आखिरी बॉल पर सिर्फ एक रन बनाना था।
लिखने वालों के लिए हर शब्द मैच की आखिरी बॉल सा होना चाहिए। मतलब बॉल फेंकने से पहले “लाइन लेंग्थ” की जांच तो करनी ही चाहिए।
मामला सिर्फ लाइन लेंग्थ का नहीं है। सवाल ये है कि एक इंसान के तौर पर बीमार शख्स के लिए स्वस्थ होने की दुआ करना हमने कब छोड़ा? ये तंगदिली आई कहां से? और कैसे इस तंगदिली ने हमारे दिमागों पर पकड़ बना ली?
सवाल मामूली नहीं
है। आखिरी कोई बात तो होगी; जो एक पत्रकार, लेखक और पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों को ऐसा सोचने के
लिए उकसा रही है।
इन सालों में ये बढ़ा
है। बात करते करते, लोग बहस पर उतारु हो रहे हैं। बहस करते
करते, कब झगड़ा कर बैठेंगे, पता नहीं चलता। बातचीत यानी चर्चा बहस के रास्ते जंग
बन गई है।
समाज के हर तबके
में ये जंग चल रही है। कोई तो है, जो बातचीत सामान्य नहीं रहने दे रहा। कौन है वो?
मैं दूसरों की
नहीं जानता; पर मेरा अनुभव है। भाई, बहन, चाचा, मामा, दोस्त और तमाम
लोगों के बीच मुद्दों पर होने वाली बातचीत सामान्य नहीं रही है।
सबने अपने लिए, एक
कोना पकड़ रखा है। सबने अपने लिए एक टीम चुन ली है। और हर शख्स ने खुद को अपनी
चुनी हुई टीम का चीयरलीडर बना लिया है।
चीयरलीडर बने शख्स
अपनी टीम के गोल पर तालियां बजाते हैं, कुर्सियों पर उछलते हैं। मोदी मोदी, राहुल
राहुल के नारे लगाते हैं। और दूसरी टीम के गोल पर गुस्से से भर उठते हैं। गालियां
देने लगते हैं। इन लोगों ने दिल में अपनी टीम के लिए बेशर्त मुहब्बत, और विरोधी
टीम के लिए नफरत ही नफरत भर रखी है।
गुस्सा लाजिमी है और नफरत भी। ये इंसानी गुण है। हर इंसान में होना ही चाहिए। पर
किसलिए? ये सवाल हमें खुद से ही पूछने हैं।
हिंसा के प्रति
गुस्सा और नफरत न पैदा होती हो, तो पढ़ना लिखना सोचना बेमानी है।
बच्चियों से रेप
पर गुस्सा न आए, तो सोचना होगा हम इंसानियत के किस पायदान पर खड़े हैं।
धर्म के नाम पर
हिंसा हो, तो गुस्सा जरुरी भाव होना चाहिए।
मंदिर मस्जिद के
नाम पर बांटने वाली राजनीति से नफरत, मैं जरुरी समझता हूं।
बुलंदशहर की तरह
पुलिसवालों को हिंसक भीड़ थाने के सामने मार डाले, तो गुस्सा आना चाहिए।
राजस्थान के अलवर
में गाय के नाम पर पहलू खान और रकबर खान की मॉब लिंचिंग पर खून खौलना चाहिए,
गुस्सा लाजिमी हो जाता है।
भूख, बिना छत, बिना
इलाज कोई इंसान मर जाए, तो ऐसी सरकारों पर गुस्सा आना चाहिए।
साल भर कड़ी धूप,
मूसलाधार बारिश और कड़ाके की सर्दी में हाड़ तोड़ने वाले किसान को उसकी फसल का मोल
न मिले, और फिर उसे फांसी पर लटकना पड़े, तो गुस्सा आना ही चाहिए।
पर गुस्से का कोई
इलाका होना चाहिए। गुस्से के पैदा होने का कोई बहाना होना चाहिए। इसे निजी हमले का
हथियार मत बनाओ।
बॉलीवुड फिल्म “घातक” के एक फिल्मी संवाद में गहरे अर्थ छिपे हैं।
जिसमें पिता बने अमरीश पुरी महात्मा गांधी के एक किस्से का जिक्र करते हुए अपने
बेटे सनी देओल से कहते हैं, “क्रोध को पालना सीख, काशी”
और शुरुआत जहां से
हुई, अंत उसी से करते हैं।
“अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उस को
छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा।“